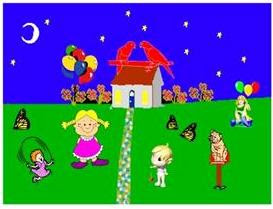समय की आवश्यकता है----पाठ्यक्रम में रंगमंच
शनिवार, 11 मई 2013
 |
| प्रसिद्ध नाटक "कहानी तोते राजा की" का एक दृश्य |
मनोवैज्ञानिकों और
समाजशास्त्रियों के अनुसार बच्चों के सर्वांगीण विकास में रंगमंच का एक बहुत बड़ा योगदान
है।यही वह माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा एक बड़े समुदाय के साथ जुड़ सकता है।जन
सामान्य के सामने अपने को प्रस्तुत करने की उसकी झिझक दूर होती है और उसकी वाक
शक्ति का विकास होता है। उसके अंदर समूह में कार्य करने के साथ ही नेतृत्व की
क्षमता भी विकसित होती है।
शिक्षा में रंगमंच की
अवधारणा कोई नई बात नहीं है। इसकी आवश्यकता का अनुभव सर्व प्रथम यूरोप में किया
गया। जहां सन 1776 में मैडम जेनेसिस ने “थिएटर आफ़ एजूकेशन” की स्थापना की और बच्चों को प्रशिक्षित करके नाटकों का
मंचन किया। इस प्रकार रंगमंच को शिक्षा में लाने की शुरुआत हुई। हमारे देश में भी
समय के साथ इसकी आवश्यकता महसूस की गयी। और सन 1965 में शैक्षिक रंगमंच की शुरुआत
हुयी।किन्तु यह प्रयास मात्र चर्चाओं और गोष्ठियों का विषय बन कर रह गया। वर्ष
1980 के बाद संगीत नाटक अकादमी,राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतेन्दु नाट्य
एकेडमी की ओर से किये गये प्रयासों से कुछ चेतना तो आई पर वह अपना कोई स्वरूप नहीं
बना पाया।
बच्चे किसी भी देश के
भविष्य होते हैं।बचपन से ही यदि उनमें रंग संस्कार पड़ जायें तो यह प्रत्यक्ष या
परोक्ष रूप से उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होगा।इस माध्यम से बच्चों में
कल्पना शक्ति,वाक्शक्ति,अनुभूति
प्रदर्शन,अभिव्यक्ति की क्षमता,चलने फ़िरने का ढंग,नेतृत्व क्षमता एवं व्यक्तिगत
कौशल का विकास होता है।रंगमंच बच्चों को जिम्मेदार बनाता है।उनमें अनुशासन के साथ
साथ समयबद्धता के गुण लाता है। यही वो तत्व हैं जो लोकतन्त्र की नींव हैं और
बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं।परन्तु यह देखकर दुख होता है कि इस विधा
का जितना लाभ बच्चों को मिलना चाहिये उतना लाभ बच्चे उठा नहीं पा रहे हैं।मात्र
गर्मी की छुट्टियों और विद्यालयों के वार्षिक उत्सवों तक बाल रंगमंच को सीमित करके
कहीं हम उनके विकास में बाधक तो नहीं बन रहे हैं? यह एक चर्चा का विषय है।
बाल रंगमंच प्रशिक्षक के
नाते यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो नाटक बच्चों के लिये मंचित किये जाते
हैं,उन्हें बच्चे बड़ी ही रुचि से देखते हैं।यदि नाटक बच्चों की मानसिकता को ध्यान
में रखकर लिखा गया है तो बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही,क्योंकि बच्चों में
अनुकरण की अपूर्व शक्ति होती है। दृश्य एवं श्रव्य –दोहरा माध्यम होने के कारण इसका प्रभाव भी दोहरा होता है।
वर्तमान समय में व्यक्ति परिवार और समाज की व्यस्तताएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गयी हैं। जिसके कारण कदम-कदम पर भटकाव बढ़ रहा है।
सामाजिक परिवेश प्रदूषित सा हो रहा है।टेलीविजन और इण्टरनेट संस्कृति का दुरुपयोग
हमें अपसंस्कृति की ओर ले जा रहा है।इसका प्रभाव बच्चों पर कुछ ज्यादा ही पड़ रहा
है। ऐसे में बाल रंगमंच जैसे सार्वजनिक और सशक्त माध्यम की प्रासंगिकता और बढ़ जाती
है। बच्चों की इसमें सीधी सहभागिता होने के कारण बच्चों में आत्मविश्वास,सृजनात्मक
क्षमता,संवेदनशीलता और टीम वर्क की भावनाएं स्वतः ही जागृत हो जाती हैं। अपनी
वाक्शक्ति के प्रदर्शन से वे आत्मविश्वास से भर जाते हैं।कभी-कभी यह भी देखा गया
है कि कुछ ऐसे बच्चे जिनमें हकलाहट की समस्या थी थियेटर ज्वाइन करने के बाद उनकी
समस्या खतम हो गयी। उनमें खोया हुआ आत्म विश्वास वापस आ गया। ऐसे बच्चों में एकाग्रता,स्मरण शक्ति भी बढ़ती है।
उनमें एक आंतरिक अनुशासन आता है। यह जागरूकता उन्हें अपने समय और परिवेश के साथ
सीधे जोड़ने का काम करती है।
एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि
बच्चा 6 वर्ष की आयु तक 40 प्रतिशत और 18 वर्ष की आयु तक 80 प्रतिशत संस्कार ग्रहण
कर लेता है। और ये संस्कार उस बच्चे के साथ जीवन भर चलते हैं।केवल 20 प्रतिशत
संस्कार ही आगे जुड़ते हैं या परिवर्तित होते हैं। बच्चों द्वारा खेले जाने वाले
बाल मनोविज्ञान पर आधारित नाटक ही सही मायनों में बाल रंगमंच कहलाता है।जटिल से
जटिल विषयों को भी रंगमंच के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। बाल रंगमंच के
विकसित न हो पाने का एक कारण और भी है। अधिकांश माता पिता रंगकर्म को पढ़ाई से अलग
मानकर उसे पढ़ाई में बाधा मानते हैं। सारा माहौल पढ़ाई और कैरियर पर ही केन्द्रित
रहता है। ऐसे में रंगमंच जैसे माध्यम को समझने या अपनाने की न तो कोई इच्छा होती
है और न ही इसके लिये अलग से कोई समय।
बाल रंगमंच का व्यापक
और प्रभावी विकास तभी हो सकता है जब इसे स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षा से अनिवार्य
रूप से जोड़ा जाए। इसकी उपादेयता को स्वीकार तो सभी करते हैं पर शासन द्वारा इस
दिशा में कोई प्रयत्न न किये जाने के कारण बात आई-गई रह जाती है।
विगत दो दशकों से बाल रंगमंच
के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। जागरूकता भी आई है। पर यह केवल कुछ बड़े शहरों तक
ही सीमित है। यदि बाल रंगमंच की संभावनाओं को कुछ अधिक व्यावहारिक आधार मिले तो
इसका विकास निश्चित ही सम्भव है। इसके लिये शासन,विद्यालय,अभिभावक तथा रंगकर्मियों
को मिलकर कुछ ठोस सामूहिक प्रयास कर अपने दायित्व निभाने होंगे।
0000
अभिनव पाण्डेय
मोबाइल-07275866955
युवा रंगकर्मी अभिनव पाण्डेय ने भारतेन्दु नाट्य एकेडमी,लखनऊ से रंगकर्म सीखा
है।अभिनव पाण्डेय ने कई टी0वी0 सीरियल्स में सहायक निर्देशक का कार्य करने के साथ
ही कुछ डाक्युमेण्ट्री फ़िल्मों का भी निर्माण किया है। टी वी से जुड़ने के बावजूद
इनका मन और दिल रंगकर्म में अधिक बसता है,खासकर बच्चों के साथ काम करना इन्हें
अधिक प्रिय है। दिल्ली,पुणे, लखनऊ,मुम्बई में काम करने के बाद फ़िलवक्त कानपुर में
रहकर बच्चों के लिये रंगमंच की पृष्ठभूमि
बनाने का काम कर रहे हैं।
·